 भारत में बकरियां, मुर्गियां या पशु पालन की प्रथा सदियों पुरानी है। बीते समय में, ग्रामीणों का मुख्य रोजगार पशु पालन होने के कारण वे इसी पर आश्रित रहते थे। लेकिन देश के विभिन्न भागों में, चारागाह भूमि और हरे चारे की कमी की वजह से पशु पालन, विशेष रुप से बकरी पालन, छोटे एवं घरेलू स्तर के पालकों के लिए कठिन हो गया है। देश के कई भागों में, बकरी पालन गैर-लाभदायक और महंगा होने के कारण अब एक अतीत बन कर रह गया है।
भारत में बकरियां, मुर्गियां या पशु पालन की प्रथा सदियों पुरानी है। बीते समय में, ग्रामीणों का मुख्य रोजगार पशु पालन होने के कारण वे इसी पर आश्रित रहते थे। लेकिन देश के विभिन्न भागों में, चारागाह भूमि और हरे चारे की कमी की वजह से पशु पालन, विशेष रुप से बकरी पालन, छोटे एवं घरेलू स्तर के पालकों के लिए कठिन हो गया है। देश के कई भागों में, बकरी पालन गैर-लाभदायक और महंगा होने के कारण अब एक अतीत बन कर रह गया है।
सामयिक प्रयास और अनुसंधान के माध्यम से किसान अनुकूल प्रौद्योगिकियों के उपयोग द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (आईआईआरएस) के कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में सराहनीय पहल की है।
वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक ईजाद की है जिसके माध्यम से मेमनों के शरीर-भार में वृद्धि के लिए बढ़े शेड में पाला जाता है जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। डॉ. एम. आनंदराज, निदेशक आईआईएसआर, कोझीकोड के अनुसार इस विधि से भूमिहीन मजदूरों और छोटे किसानों को लाभ पहुँच रहा है। इतना ही नहीं, हरे चारे की कमी का मुकाबला करने के लिए वैज्ञानिक और कम लागत वाली प्रक्रिया भी विकसित कर ली गई है।





इस उद्देश्य के लिए कोई विशेष नस्ल निर्धारित नहीं की गई है। किसी भी स्थानीय नस्ल के मेमनों (दोनों नर व मादा) को इस पद्धति के माध्यम से चयन करके पाला जा सकता है।
इस उद्देश्य के लिए कोई विशेष नस्ल निर्धारित नहीं की गई है। किसी भी स्थानीय नस्ल के मेमनों (दोनों नर व मादा) को इस पद्धति के माध्यम से चयन करके पाला जा सकता है।
बकरी फ़ीड बाजार में उपलब्ध हो सकता है या किसान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके स्वयं फ़ीड मिश्रण तैयार कर सकते हैं।
मेमनों के स्वस्थ विकास के लिए, पहली डी-वर्मिंग ब्रायलर पालन के 45वें दिन पर किया जाना चाहिए। डी-वर्मिंग हर महीने दोहराया जाना चाहिए।
विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूह जैसे कावेरी, कुटम्बाश्री और निधि एवं केरल में कोझीकोड जिले में स्थित पेरुवान्नामुजी के अन्य किसान भी इस प्रक्रिया का पिछले पाँच सालों से प्रयोग कर रहे हैं। समूह के सदस्यों के अनुसार यह विधि उन किसानों के लिए उपयुक्त है जिनके पास पशुओं के चरने लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। यह प्रौद्योगिकी किसानों को कम समय में अधिक संख्या में बकरी पालन करने में मदद करती है।
"अब यह तकनीक इस केन्द्र का एक प्रमुख कार्यक्रम बन गयी है। इस तकनीक की सफलता अकेले केरल तक ही सीमित नहीं है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों से किसान इन स्वयं सहायता समूहों का दौरा उनकी सफलता का फार्मूला जानने के लिए कर रहे हैं। डॉ. टी.अरुमुघनाथन, कार्यक्रम समन्वयक, के.वी.के. पेरुवन्नामुजी का कहना है कि हाल ही में विदेशों से भी इस प्रक्रिया को लेकर लोगों ने अपनी जिज्ञासा जाहिर की है।"
(स्रोत: एनएआईपी मास मीडिया परियोजना डीकेएमए , कंसोर्टियम साथी , आईआईएसआर, कोझाकोड से जानकारी के साथ)
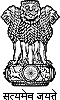







Like on Facebook
Subscribe on Youtube
Follow on X X
Like on instagram