 उज्जैन जिले में सोयाबीन आधारित फसल पद्धति प्रमुखता से अपनायी जाती है। खरीफ में लगभग 95 प्रतिशत क्षेत्र में सोयाबीन उगाने के पश्चात रबी मौसम में चना, गेहूं, आलू, लहसुन और प्याज की खेती की जाती है। पहले किसान टमाटर की खुला परागित किस्में उगाते थे और इसकी उत्पादन प्रौद्योगिकी पर ध्यान न देने के कारण केवल 150 क्विंटल प्रति हैक्टर की कम उपज ही प्राप्त होती थी। कृषि विज्ञान केन्द्र, उज्जैन ने क्षमतावान क्षेत्र की पहचान करके वर्ष 2007 में संकर टमाटर की खेती को प्रोत्साहित किया। इसमें संकर किस्में, नर्सरी प्रबंधन, समन्वित पोषण और कीट प्रबंधन, पौध उगाने के लिए ट्रे का उपयोग जैसी अनुकूल प्रौद्योगिकियों के प्रयोग और टमाटर में विकृतियों को दूर करने के लिए विशेष हस्ताक्षेप भी किया गया। अब उज्जैन जिले में 3500 हैक्टर क्षेत्र पर टमाटर की खेती की जाती है और 250 से 325 क्विंटल प्रति हैक्टर औसत उपज प्राप्त होती है।
उज्जैन जिले में सोयाबीन आधारित फसल पद्धति प्रमुखता से अपनायी जाती है। खरीफ में लगभग 95 प्रतिशत क्षेत्र में सोयाबीन उगाने के पश्चात रबी मौसम में चना, गेहूं, आलू, लहसुन और प्याज की खेती की जाती है। पहले किसान टमाटर की खुला परागित किस्में उगाते थे और इसकी उत्पादन प्रौद्योगिकी पर ध्यान न देने के कारण केवल 150 क्विंटल प्रति हैक्टर की कम उपज ही प्राप्त होती थी। कृषि विज्ञान केन्द्र, उज्जैन ने क्षमतावान क्षेत्र की पहचान करके वर्ष 2007 में संकर टमाटर की खेती को प्रोत्साहित किया। इसमें संकर किस्में, नर्सरी प्रबंधन, समन्वित पोषण और कीट प्रबंधन, पौध उगाने के लिए ट्रे का उपयोग जैसी अनुकूल प्रौद्योगिकियों के प्रयोग और टमाटर में विकृतियों को दूर करने के लिए विशेष हस्ताक्षेप भी किया गया। अब उज्जैन जिले में 3500 हैक्टर क्षेत्र पर टमाटर की खेती की जाती है और 250 से 325 क्विंटल प्रति हैक्टर औसत उपज प्राप्त होती है।
मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण किसान अपनी फसल कम दामों पर बेचने को मजबूर थे और कभी-कभी तो इसका दाम 2 से 3 रुपये प्रति कि.ग्रा. तक ही मिल पाता था। इसके मद्देनजर कृषि विज्ञान केन्द्र ने इसमें पहल की ताकि कुल उपज का लगभग 35 प्रतिशत भाग घरेलू उत्पादों के रूप में संरक्षित किया जा सके। इसके लिए देवराखेड़ी, भेसोडा और कपेली गांवों से एक टमाटर उत्पादन समूह का चुनाव किया गया। टमाटर परिरक्षण के लिए इन गांवों में कई तरह के प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। कृषक महिलाओं को टमाटर उत्पादों के परिरक्षण का व्यवहारिक प्रदर्शन किया गया। 'कैचअप' तैयार करने के लिए चयनित पौधों पर टैग लगा दिये गये।


इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप वर्ष 2008 में 1.2 और 1.5 लाख पूंजी एकत्र करके दो स्वयं सहायता संगठन बनाये गये- 'ओजन स्वयं सहायता समूह' और 'जय मां दुर्गा'। कृषि विज्ञान केन्द्र की गृह वैज्ञानिक के मार्गदर्शन में कृषक महिलाओं ने घरेलू स्तर पर टमाटर कैचअप बनाना सीखा। स्वयं सहायता समूह की क्षमता और विपणन के मद्देनजर कृषि विज्ञान केन्द्र ने इन उत्पादों को बड़े स्तर पर बेचने के लिए इनका ब्रांड नाम 'राज विजय टमाटर कैचअप' रखा। यह 'राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा विपणन हेतु उत्पादों का संक्षिप्त नाम है। तीन वर्ष के अग्रिम प्रदर्शनों के पश्चात टमाटर उत्पादन और परिरक्षित उत्पादों का आर्थिक विश्लेषण किया गया जिससे पता लगा कि कृषकों को 9.8 गुना अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है।
अब ये दोनों समूह 200 से 2500 कि.ग्रा. उत्पाद देने में सक्षम हैं। अगले वित्तीय वर्ष में बैंक ऑफ इंडिया की वित्तीय सहायता से इन समूहों द्वारा एक लघु प्रसंस्करण इकाई शुरू करने की योजना है। जिला स्तर पर कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों का आर्थिक स्तर सुधारने के लिए उचित प्रौद्योगिकी और प्लेटफार्म प्रदान करते हैं।
(स्रोतः कृषि विज्ञान केन्द्र, उज्जैन)
(हिन्दी प्रस्तुतिः एनएआईपी मास मीडिया परियोजना, कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय, आईसीएआर)
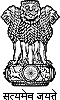







Like on Facebook
Subscribe on Youtube
Follow on X X
Like on instagram