 केरल का मुख्य चावल भंडार वाला कुट्टनाड विश्व के उन क्षेत्रों में से एक है जहां समुद्र के औसत तल के नीचे चावल उत्पन्न किया जाता है। यह एक अनूठी पारिस्थितिक रूप से नाजुक जैव-भौगोलिक इकाई के रूप में जाना जाता है जिसका अधिकांश भाग अलापुज्जा जिले में स्थित है। इस प्रणाली के नाजुक होने का कारण जलाक्रांतता तथा मृदा के लवणीय होने के साथ-साथ यहां की जलवायु में होने वाले उतार-चढ़ाव हैं। निचले धान के खेतों में ग्रीष्मकालीन वर्षा तथा मानसून के दौरान बाढ़ से होने वाली फसलों की क्षति जिसे स्थानीय भाषा में पदाशेखराम कहा जाता है, यहां बहुत सामान्य है। जैव-भौगोलिक तथा सम्बद्ध सामाजिक कारकों के इस अनूठेपन के कारण इस क्षेत्र को वर्ष 2003 में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली (जीआईएएचएस) का दर्जा दिया गया। इस विरासत के दर्जे के कारण जलाक्रांत प्रणाली की पारिस्थितिकी को पुन: सुधारने और इसे टिकाऊ बनाने का काम आवश्यक है। इसमें शामिल होने वाले अन्य कारण हैं : इस क्षेत्र के किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरकों तथा पादप सुरक्षा संबंधी रसायनों का गैर समझे-बूझे उपयोग जिसके कारण फसलें तो प्रभावित हुई ही हैं, पर्यावरण भी प्रदूषित हुआ है। अधिक मात्रा में बीजों के उपयोग तथा मजदूरी की उच्च लागत के कारण खेती की लागत बढ़ गई है तथा धान उगाने वाले किसानों को बहुत कम लाभ हो रहा है।
केरल का मुख्य चावल भंडार वाला कुट्टनाड विश्व के उन क्षेत्रों में से एक है जहां समुद्र के औसत तल के नीचे चावल उत्पन्न किया जाता है। यह एक अनूठी पारिस्थितिक रूप से नाजुक जैव-भौगोलिक इकाई के रूप में जाना जाता है जिसका अधिकांश भाग अलापुज्जा जिले में स्थित है। इस प्रणाली के नाजुक होने का कारण जलाक्रांतता तथा मृदा के लवणीय होने के साथ-साथ यहां की जलवायु में होने वाले उतार-चढ़ाव हैं। निचले धान के खेतों में ग्रीष्मकालीन वर्षा तथा मानसून के दौरान बाढ़ से होने वाली फसलों की क्षति जिसे स्थानीय भाषा में पदाशेखराम कहा जाता है, यहां बहुत सामान्य है। जैव-भौगोलिक तथा सम्बद्ध सामाजिक कारकों के इस अनूठेपन के कारण इस क्षेत्र को वर्ष 2003 में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली (जीआईएएचएस) का दर्जा दिया गया। इस विरासत के दर्जे के कारण जलाक्रांत प्रणाली की पारिस्थितिकी को पुन: सुधारने और इसे टिकाऊ बनाने का काम आवश्यक है। इसमें शामिल होने वाले अन्य कारण हैं : इस क्षेत्र के किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरकों तथा पादप सुरक्षा संबंधी रसायनों का गैर समझे-बूझे उपयोग जिसके कारण फसलें तो प्रभावित हुई ही हैं, पर्यावरण भी प्रदूषित हुआ है। अधिक मात्रा में बीजों के उपयोग तथा मजदूरी की उच्च लागत के कारण खेती की लागत बढ़ गई है तथा धान उगाने वाले किसानों को बहुत कम लाभ हो रहा है।
इस समस्याओं को हल करने के लिए भा.कृ.अनु.प. – केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान (सीपीसीआरआई) की मेजबानी में कृषि विज्ञान केन्द्र - अलापुज्जा द्वारा वर्ष 2011 से 2015 तक लगातार चार फसल मौसमों में (एक वर्ष में केवल एक फसल लेना ही संभव है) जलवायु समुत्थानशील कृषि पर राष्ट्रीय पहल (एनआईसीआरए) के अंतर्गत वेलियानाड ब्लॉक के मुत्तार गांव में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन आयोजित किए गए।



किसानों को (i) ड्रम सीडर के माध्यम से बीजों व पौधों की संख्या को उपयुक्ततम बनाने, मृदा परीक्षण पर आधारित स्थल विशिष्ट अम्लता प्रभावी क्षेत्रों में पोषक तत्वों का प्रबंध करने और बीजोपचार के लिए स्यूडोमोनास के उपयोग के माध्यम से रोग प्रबंध करने, प्रमुख नाशीजीवों – तना बेधक और पत्ती मोड़क कीटों के लिए ट्राइकोकार्ड रखने और कीटनाशियों को पत्तियों पर छिड़कने, नाशीजीवों की निगरानी के लिए प्रकाश फंदों का प्रयोग करने तथा चावल के मत्कुणों को नष्ट करने के लिए मत्स्य अमीनो अम्ल का इस्तेमाल करने पर प्रदर्शनों के पैकेज अपनाने की सुविधा प्रदान की गई। कुल 114 किसानों ने इन चार वर्षों के दौरान इन प्रदर्शनों में भाग लिया और ये प्रदर्शन 74.2 हैक्टर क्षेत्र में लगाए गए।
प्रमुख प्रभाव
- धान रोपाई यंत्र (ड्रम सीडर) का उपयोग करके बीज की आवश्यकता 100-120 कि.ग्रा./है. से कम करके 30 कि.ग्रा./है. की गई क्योंकि पहले किसान छिड़ककर बीज बोते थे। इस प्रकार बीज पर लगने वाली लागत लगभग 25 प्रतिशत रह गई। फसल में वायु के आसानी से व पर्याप्त रूप से आने-जाने के कारण फसल की नाशीजीवों व रोगों के प्रति संवेदनशीलता में भी कमी आई। पौधों की मिट्टी पर अच्छी पकड़ बनी जिससे वे गर्मियों के मौसम के दौरान होने वाली वर्षा और हवा के कारण कटाई की अवस्था के दौरान गिरे भी नहीं। इस प्रकार, परंपरागत छिड़ककर बोई गई फसल के पौधों के गिर जाने के कारण फसल को जो क्षति होती थी वह भी 20 प्रतिशत कम हो गई। इन सभी कारकों से खेती की लागत में लगभग 10-15 प्रतिशत की कमी आई।
- डोलोमाइट का उपयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करने से मृदा की अम्लता में कमी आई तथा फसलों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ी लेकिन इसके लिए मैग्नीशियम की आपूर्ति भी जरूरी हुई। मृदा परीक्षणों के आधार पर उर्वरकों की लागत में भी 30 प्रतिशत कमी हुई।
- प्रदर्शन के इन प्लॉटों में नाशीजीवों और रोगों का कोई प्रकोप नहीं हुआ और किसान स्यूडोमोनास तथा ट्राइकोकार्ड के प्रभाव से संतुष्ट थे। इन विधियों को अपनाने से न केवल खेती की लागत कम हुई बल्कि पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आई।
- कुल मिलाकर प्रौद्योगिकियों के इस पैकेज से उपज में औसतन 15-20 प्रतिशत की व़ृद्धि हुई। जहां एक ओर छिड़ककर उगाई गई परंपरागत विधि से किसानों को औसतन 5-6 टन/है. उपज मिलती थी, वहीं इन प्रौद्योगिकियों से निवेशों का कम उपयोग करते हुए किसानों ने 6-7 टन/है. उपज ली। प्रदर्शन प्लाटों में प्रति वर्ग मी. उत्पादक दोजियों की संख्या तथा प्रति पुष्पगुच्छ दानों की संख्या सभी चारों वर्षों के दौरान अधिक रही तथा इस अवधि में इन प्लॉटों में ली गई फसलों के दाने भी भारी थे। प्राप्त की गई उच्च उपज तथा खेती की लागत में कमी आने से किसानों को प्रति हैक्टर कम से कम 12,500/-रु. का शुद्ध उच्चतर लाभ हुआ। साझेदार किसान बहुत प्रसन्न थे और इनमें से अनेक आस-पास के गांवों के प्रगतिशील किसानों के बीच प्रौद्योगिकियों के इस पैकेज के प्रचार-प्रसार के लिए मास्टर कृषक के रूप में कार्य कर रहे हैं।
(स्रोत: भा.कृ.अनु.प. – केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड)
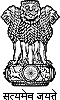







Like on Facebook
Subscribe on Youtube
Follow on X X
Like on instagram