पश्चिम बंगाल के लाल और लेटराइटिक क्षेत्र में उप-उष्णकटिबंधीय जलवायु का पाया जाना यहां की विशेषता है तथा यहां औसत वार्षिक वर्षा 1000-1200 मिमी (जून-सितंबर के दौरान प्राप्त वर्षा का 80%) और तापमान 16-420 सेंटीग्रेड के बीच होता है। यहां की भूमि की प्रक़ति लहरदार (अनड्यूलेटेड) होने के कारण ऊपरी मिट्टी में क्षरण होता है जिससे एन, पी, के और जैविक पदार्थ का खराब स्तर पाया जाता है । मृदा की बनावट रेतीली से लेकर बलुई दुमट प्रकार की है जिसमें लोहा और एल्यूमीनियम प्रचुर मात्रा में किंतु कैल्शियम, मैगनीज, बोरान और एमओ कम मात्रा में पाया जाता है । मिट्टी की जल प्रतिधारण क्षमता कम है और मृदा की पीएच 5 से 5.5 के बीच होती है। इस अंचल में अधिकतर रबी-गर्मी में बोरो चावल और खरीफ सीजन में अमन चावल की खेती की जाती है। बोरो चावल की खेती के तहत क्षेत्र दिन प्रतिदिन घट रहा है क्योंकि अनियमित, असमान और कम वर्षा के कारण भूजल का स्तर हर साल गिर रहा है। फिर भी इस अंचल में फसल का प्रमुख पैटर्न धान-धान-परती है।
पश्चिम मिदनापुर जिले का एक बड़ा हिस्सा ऐसे लाल और लेटराइटिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहां फसल-प्रणाली धीरे-धीरे धान-परती-परती में बदल रही है। बोरो चावल की खेती के अंतर्गत क्षेत्र में हुई कमी के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए किसानों को एक व्यवहार्य विकल्प की नितांत आवश्यकता थी। कहीं कहीं पर कुछ किसानों ने वैकल्पिक तौर पर कई अन्य फसलों और सब्जियों को उगाने की कोशिश की, लेकिन बोरो चावल को प्रतिस्थापित करने के लिए कोई टिकाऊ फसल न मिलने पर उनका मोहभंग हुआ। पश्चिम मेदिनीपुर के जामरासुली, धुलीपुर, अस्थापारा और तुरा के चार गांवों के किसानों के एक समूह ने 2005-06 के दौरान केवीके से संपर्क किया और इस क्षेत्र के लिए वैकल्पिक फसल खोजने की सलाह मांगी, ताकि उन्हें उत्पादकता और बिक्री के रुप में एक सुनिश्चित आय की प्राप्ति हो सके। समस्या की गंभीरता को समझते हुए, केवीके ने गांवों में पीआरए के माध्यम से कृषि-पारिस्थितिक तंत्र विश्लेषण को अपनाया ताकि खेती की मौजूदा स्थिति के लक्षणों का पता लगाकर खेतिहर किसानों की जरूरत के अनुसार नई फसल लेने की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। दौरों, किसानों के साथ बातचीत और विस्तृत सर्वेक्षण ने केवीके को ऐसी फसल की पहचान करने में मदद की जो मौजूदा जलवायु के अनुरूप हो। अंत में, केवीके ने चयनित गांवों में उस क्षेत्र के लिए वैकल्पिक फसल के तौर पर 'मूंगफली' की फसल लेने का फैसला किया। मूंगफली की खेती को प्रारंभ करने से पहले संबंधित विभाग से नमी, धूप, बादलों के दिनों आदि पर विस्तृत मौसम संबंधी वास्तविक जानकारी भी एकत्र की गई थी।
प्रौद्योगिकी, कार्यान्वयन और समर्थन
केवीके ने प्रारंभिक वर्षों में मूंगफली की चार किस्मों अर्थात् टीपीजी -41, टीजी -26, टीजी -38 बी और TAG-24 के प्रदर्शन का उन गांवों के कई स्थानों में मूल्यांकन किया ताकि इस कृषि-जलवायु वाली दशाओं के लिए स्थिति सबसे अधिक उपयुक्त किस्म की पहचान की जा सके। किस्मों के मूल्यांकन के पश्चात बीज जनित बीमारियों और कीट नियंत्रण के उपायों का प्रदर्शन किया गया। संबंधित विभागों के विस्तार कार्यकर्ता खेती की प्रक्रियाओं के प्रमाणीकरण में संलग्न रहे। अंतत: केवीके द्वारा टीएजी -24 किस्म की खेती के लिए पूर्ण पैकेज की सिफारिश की जिसमें @ 750 / हेक्टेयर की दर से राइजोबियम द्वारा बीजोपचार, बुवाई के 30 दिनों के बाद 500 किग्रा/हेक्टेयर की दर से मिट्टी में जिप्सम का उपयोग करना तथा बुवाई के 15 से 30 दिनों के बाद 2.0 ग्राम/लीटर की दर से बोरिक एसिड का छिड़काव तथा एफिड का प्रबंधन सम्मिलित है। टीएजी-24 किस्म के साथ रबी-ग्रीष्म ऋतु के दौरान 10 हेक्टेयर क्षेत्र में अग्र पंक्ति के संचालन द्वारा केवीके ने इस पैकेज का फिर से प्रदर्शन किया गया था। किसानों ने रू0 25000 / हेक्टेयर की शुद्ध आय के साथ 20 कुन्तल/ हेक्टेयर की औसत उपज प्राप्त की । इस सफलता से प्रोत्साहित होकर केवीके ने अगले खरीफ सीजन के दौरान एफएलडी आयोजित करके 12 कुन्तल/हेक्टैयर की उपज और रू0 16000 / हेक्टेयर का शुद्ध लाभ प्राप्त किया।
अंगीकरण, प्रसार और लाभ
धीरे-धीरे इस प्रौद्योगिकी का क्षैतिजक प्रसार प्रारंभ हुआ और अगले तीन वर्षों में 150 हेक्टेयर क्षेत्र को मूंगफली की खेती के तहत शामिल किया गया। बोरो धान की खेती में किसानों के लिए एक गंभीर समस्या 16-20 सिंचाई द्वारा 50-60 एकड़-इंच पानी की आवश्यकता भी रही है। हालांकि, मूंगफली की खेती, केवल 10-12 एकड़-इंच पानी (4-5 सिंचाई) से ही संभव थी जो कि किसानों के लिए वहनीय थी। इसके अलावा, मूंगफली की खेती का मिट्टी के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव होता है, इसकी खेती में अधिक श्रम-दिवस लगते हैं जिससे ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों का प्रवास घटता है। मिट्टी के विश्लेषण से इस बात का संकेत मिलता है कि मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन को 180 किलो/हेक्टेयर से 210 किलो/हेक्टेयर तक बढाने तथा उपलब्ध जैविक पदार्थ की प्रतिशतता को 0.5% से 0.75% तक करने पर मिट्टी की पीएच को 4.8 से 5.6 तक बदला जा सकता है। इस अवधि के दौरान, 10,500 की संख्या तक अतिरिक्त मानव दिवसों का सृजन हुआ जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों के प्रवास में 30% की कमी आई। पश्चिम मेदिनीपुर तथा इसके आस-पास के जिलों में मूंगफली का अच्छा बाजार है, जिससे किसानों को मूंगफली की खेती से तत्काल आय की प्राप्ति हुई और वे मूंगफली की खेती करने को प्रोत्साहित हुए। मूंगफली की खेती पश्चिम मेदिनीपुर जिले तक ही सीमित नहीं है। पुरुलिया और बांकुरा जिलों में समान कृषि-जलवायु स्थितियों के किसानों ने बोरो चावल के स्थान पर मूंगफली को अपनाना शुरू कर दिया है।
(स्रोत: कृषि विज्ञान केंद्र, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल)
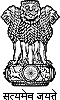







Like on Facebook
Subscribe on Youtube
Follow on X X
Like on instagram