वर्ष 2009 में पटियाला के बुधमौर और जोधपुर गांवों के किसानों के एक समूह ने लवणता से प्रभावित फसलों के कारण उपज में हानि का सामना करते हुए आईसीएआर- केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल के वैज्ञानिकों से संपर्क किया। उन्होंने विस्तार से इस बात को बताया कि कैसे भूजल क्षारीयता में लगातार वृद्धि हुई है और इससे जनित भूमि गिरावट से उनकी जिंदगी में एक ठहराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। चावल और गेहूं की खेती में बार-बार फसल की विफलता, पौधों की व्यापक तौर पर मृत्यु, पीला पड़ना, प्रजनन बंध्यता और दानों के न बन पाने (पुअर सेटिंग) की समस्या एक आम बात हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप औसतन (30-40%) उपज का नुकसान हो रहा था। इस समस्या की प्रकृति और सीमा को समझने के लिए प्रभावित गांवों के दौरे हेतु वैज्ञानिकों की एक बहु-विषयी टीम गठित की गई थी। इसके बाद, प्रभावित किसानों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा (प्रोफाइल) के साथ-साथ प्रभावित भूमि से मिट्टी और सिंचित जल के नमूनों को इकट्ठा करने के लिए बार-बार दौरे किए गए ताकि उपयुक्त नैदानिक उपायों का सुझाव दिया जा सके और उन्हें कार्यान्वित किया जा सके। जोधपुर और बुधमौर गांवों के प्रभावित खेतों से मिट्टी और सिंचित जल के नमूनों के नैदानिक उपायों में मिट्टी की भारी बुनावट (गाद+चिकनी मिट्टी ~ 80.0%), उच्च पीएच2 (8.5-9.5), मध्यम लवणता (ईसी2 0.7-0.9) और भूजल में उच्च आरएससी (3.5-4.1 meq L-1) का पता चला। मृदा में जैविक कार्बन, उपलब्ध नाइट्रोजन और उपलब्ध पी (तालिका 1) में भी कमी पाई गई ।
तालिका एक. अध्ययन क्षेत्र में क्षारीयता प्रभावित भूमि के भौतिक-रासायनिक गुण
|
मृदा (0-15 सेमी) (एन = 28) |
जल (एन = 9) |
|||||||
|
मृदा पीएच 2 |
मृदा ईसी 2 |
जैविक कार्बन (%) |
उपलब्ध एन (किलो/ हे0) |
उपलब्ध P2O5 (किलो/ हे0) |
उपलब्ध K2O (किलो/ हे0) |
आरएससी meq L-1 |
पीएच |
ईसी (dSm-1) |
|
8.5-9.5 |
0.7-0.9 |
0.4-0.5 (कम) |
143.9 (कम) |
21.2 (कम) |
228.8 |
3.5-4.1 |
7.8-8.2 |
0.7-0.8 |
चयनित किसानों को मिट्टी और जल विश्लेषण के प्रारंभिक परिणाम बताए गए थे। पहली बार प्रभावित किसानों को ‘सिंचाई के पानी में' आरएससी समस्या ’ के बारे में पता चला, जो भूमि में गिरावट और खराब फसल उपज के वास्तविक अंतर्निहित कारणों में से प्रमुख था। इसके अलावा, समस्या के बारे में वैध निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए लगातार चार वर्षों (200 9 -2012) तक एक सहभागिता अनुसंधान योजना संचालित की गई। इस सफलता गाथा के कांसेप्ट लीडर (डॉ रंजय के सिंह) ने वैज्ञानिकों की एक बहुविषयी टीम (डॉ आरके यादव, डॉ सत्येंद्र कुमार, डॉ अंशुमन सिंह, डॉ अरविंद कुमार और डॉ अवतार सिंह) के साथ मिलकर विभिन्न परियोजनाओं और गतिविधियों के माध्यम से विविध इंटरवेंशन (हस्तक्षेप) किए और उनकी सफलता का आकलन किया। परिणामों से इस बात का संकेत मिलता है कि chiseling (चिसलिंग) द्वारा बासमती सीएसआर-30 और पूसा-44 की अनाज उपज में क्रमश: 8.0% और 10.0% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, लेजर लेवलिंग को अपनाने से सीएसआर-30 में 12.0% और पूसा-44 में 15% तक पैदावार में वृद्धि हुई। इसके विपरीत, जब उच्च आरएससी युक्त सिंचित जल को जिप्सम की क्यारियों (ट्यूब-वैल के कक्ष में रखा हुआ) के माध्यम से सींचा गया तो पूसा-44 (2 9 .0%) की तुलना में अनाज की उपज में सीएसआर-30 (37.0%) में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि पाई गई थी।
चावल की खेती में सफलता
मिट्टी के क्षारयुक्त होने और सिंचित जल में आरएससी अधिक होने पर किसानों की कृषि आय को स्थाई तौर पर बनाए रखने के लिए चावल (सीएसआर-36 और सीएसआर-30) और गेहूं (केआरएल-210) की खेती में बेहतर प्रबंधन प्रक्रियाओं और लवणता के प्रति सहिष्णु किस्मों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था। इन प्रयासों के कारण, 35 चयनित किसानों में से, ≈60.0% किसानों ने प्रभावित भूमि में जिप्सम का उपयोग किया, 40.0% ने लेजर लेवलिंग को अपनाया, 15.0% ने चिसीलिंग को परखा और 5.0% ने सिंचित जल में आरएससी को बेअसर करने के लिए जिप्सम-बेड तकनीक को अपनाया। चावल की औसत पैदावार सीएसआर -36 और पूसा -44 में क्रमश: ≈4.4 और 4.0 टन प्रति हेक्टेयर थी (चित्र 1)। जो पूसा-44 की अपेक्षा सीएसआर-36 में ≈10.0% तक की उपज वृद्धि को दर्शाती है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अध्ययन क्षेत्र में कुछ किसानों ने 2007-2008 में इन हस्तक्षेपों के शुरू होने से कुछ ही समय पहले बासमती चावल सीएसआर-30 को अपनाया था किंतु वे जिप्सम आधारित प्रौद्योगिकी को न अपनाने के कारण संतोषजनक उपज प्राप्त करने में असफल रहे। इसके बाद, या तो मिट्टी में या सिंचित जल के माध्यम से जिप्सम का उपयोग करने पर सीएसआर-30 की उपज में काफी सुधार हुआ जिससे किसानों को वर्ष 2010 से (चित्र 2) 2.1 टन/हेक्टेयर अनाज उपज लेने में सफलता मिली।
गेहूं में सफलता
चावल की खेती में आश्चर्यजनक सफलता से सीख लेते हुए, इसी तरह की दशाओं में गेहूं की उपज को बढ़ाने के प्रयास शुरू किए गए। इस इलाके में वर्ष 2008-2012 के दौरान किसानों ने गेहूं की किस्म पीबीडब्ल्यू -343 की खेती करके 3.8 टन/हेक्टेयर की औसत पैदावार प्राप्त की। वर्ष 2013-2017 के दौरान, कई किसानों ने एचडी-2967 की खेती शुरू की जिससे 4.4 टन/ हेक्टेयर ( चित्र 3 ) की अपेक्षाकृत उच्च औसत पैदावार प्राप्त हुई । इसी बीच वर्ष 2015 में कुछ चयनित किसानों के खेतों पर लवणता-सहिष्णु गेहूं की किस्म केआरएल-210 का प्रदर्शन किया जहां इस किस्म ने पीबीडब्ल्यू -343 और एचडी -2967 दोनों किस्मों से बेहतर प्रदर्शन किया। मृदा पीएच तथा सिंचित जल आरएससी की आदर्श दशाओं में केआरएल-210 (4.9 टन/हेक्टेयर) किस्म से प्राप्त औसत दाना उपज को पीबीडब्लू-343 और एचडी-2967 की तुलना में क्रमशः ≈ 29.0% और 10.0% अधिक पाया गया। अध्ययन के अंतर्गत किसानों में से अधिकांश (85.0%) ने बताया कि जिप्सम-बेड प्रौद्योगिकी को अपनाने में सरकारी सब्सिडी का न मिलना एक प्रमुख बाधा थी जिसमें विशेष कक्षों को बनाने के लिए एक बार में ≈ रुपये 35,000 /यूनिट का एकमुश्त निवेश शामिल है। परिणामस्वरूप, संभावित लाभ के बारे में पता होने के बावजूद छोटे और मझोले किसानों में से अधिकतर इस तकनीक को अपनाने में असमर्थ हैं। तुलनात्मक रूप में, लेजर लैंड लेवलिंग को अधिक अपनाने का कारण इसकी लागत का कम होना (≈ रू0 3000/ हेक्टेयर) जिसे प्रत्येक तीसरे वर्ष में किराए पर लेकर (कस्टम हायरिंग) द्वारा व्यय किया जाता है।
नीतिगत शिक्षा (पॉलिसी लेसन)
पटियाला जिले के किसानों के साथ मिलकर किए गए परीक्षणों के दौरान प्राप्त अनुभव से पता चलता है कि मिट्टी की क्षारीयता, निम्न प्रजनन क्षमता, सिंचित जल में उच्च आरएससी और जलवायु में विविधता सहित कई प्रकार के दबावों से ग्रस्त इलाकों में एकल तकनीक (सिंगल तकनीक) से वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। यह समय की मांग है कि अध्ययन के तहत इलाकों में लवणता से प्रभावित भूमि से उत्पादकता प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक सिद्ध प्रौद्योगिकियों (प्रूवेन) के एकीकृत उपयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि तकनीकी युक्तियों (इंटरवेंशन) से लवणता और क्षारीयता वाली मिट्टी की उत्पादकता में कई गुना वृद्धि लाई जा सकती है, बशर्तें कि वैज्ञानिकों और विस्तार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किसान सक्रिय रूप से खेती का कार्य करें। क्षारीयता, ताजे जल की कमी और जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रतिकूल प्रभावों के अंतर्गत आने वाले बड़ी संख्या में किसानों के बीच उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकृत पैकेज को तेजी से अपनाने के लिए पंजाब सरकार और आईसीएआर-सीएसएसआरआई के बीच करार (एमओयू) की जरूरत महसूस की जा रही है ।
(स्रोत : आईसीएआर-केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल -132001, हरियाणा)
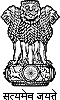







Like on Facebook
Subscribe on Youtube
Follow on X X
Like on instagram