झारखंड में फलों की महत्त्वपूर्ण फसलों में से एक पपीता मुख्य रूप से राज्य में घरों के पिछवाड़े बगीचों में उगाया जाता है। भले ही किसानों द्वारा वासभूमि में उगाया और खाया जा रहा हो, लेकिन राज्य के आदिवासी किसानों के बीच वैज्ञानिक पपीता की खेती प्रारंभिक अवस्था में है।


इस अंतर को पाटने के उद्देश्य से झारखंड के गुमला, रांची और लोहरदगा जिले में भाकृअनुप- आरसीईआर के कृषि प्रणाली अनुसंधान केंद्र, रांची ने 2018-19 के दौरान वैज्ञानिक पपीते की खेती पर प्रौद्योगिकी प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन फलों पर भाकृअनुप-अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के जनजातीय उप योजना के तहत किया गया था।

जनजातीय किसानों को जुटाने के लिए कृषि आजीविका के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन प्रदान (प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन) ने ठोस समर्थन दिया। पौधों के रोपण से पहले वैज्ञानिक पपीते की खेती पर जनजातीय किसानों के संसर्ग दौरों के साथ-साथ लगभग 8 व्यापक क्षेत्र प्रशिक्षण किए गए। लगभग 1,300 जनजातीय किसानों को प्रशिक्षण दिया गया।
पपीते की किस्मों - रेड लेडी, एनएससी 902 और रांची लोकल के साथ प्रौद्योगिकी प्रदर्शन को 600 से अधिक जनजातीय किसानों के खेतों (30,000 पौधों) में किया गया था। कीट और बीमारियों के लिए तुलनात्मक रूप से कम संवेदनशीलता और इसकी कठोरता के कारण किसान मुख्य रूप से पिछवाड़े के बागानों में रांची लोकल किस्म उगा रहे थे। लेकिन, एक ही समय में स्वाभाविक रूप से एक लिंगाश्रयी से केवल 50%-60% पौधे फल पैदा करते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए किसानों के खेतों में ‘प्रति गड्ढे तीन रोपण और फूलों की दीक्षा के बाद नर पौधों को हटाने’ पर प्रौद्योगिकी प्रदर्शन किया गया। इस प्रथा ने 80%-90% फलवाले पौधे दिए और अंततः रांची लोकल किस्म के रोपण की पारंपरिक विधि पर उत्पादन में 30%-40% की वृद्धि की।
लोहरदगा जिले के डुबांग गाँव की श्रीमती रूपवंती दीदी ने लगभग 200 मीटर2 के एक क्षेत्र में उपरोक्त सिफारिशों के अनुसार रांची लोकल के 45 पपीते के पौधे लगाए। इसके फलस्वरूप उसे 38 फलदार पौधे प्राप्त हुए और पौधों के 5 से 7 महीने की उम्र के बाद उसने वनस्पति प्रयोजन पपीता बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी उपज का लगभग 65% सब्जी पपीता के रूप में बेचा, जिसकी शुद्ध आय 8,550 रुपए और बाकी उपज को रोपण के 10-13 महीने के बाद पके हुए फल के रूप में 7,400 रुपए की शुद्ध आय के साथ बेच दिया। इस तरह उसने पपीते की किस्म - रांची लोकल - की खेती से कुल 15, 950 रुपए कमाए।
सूक्ष्म पोषक तत्त्व अनुप्रयोग, विशेष रूप से बोरान आवेदन (0.3%) का प्रदर्शन भी किसानों के बीच किया गया। बोरान अनुप्रयोग (4 स्प्रे) ने फूल और फलों की बूँद के बहाव को 22%-35% तक कम कर दिया और किस्मों की परवाह किए बिना उपज को 15%-20% तक बढ़ा दिया। वेक्टर के माध्यम से इस क्षेत्र में एक बड़ी बीमारी पपीता रिंग स्पॉट वायरस (पीआरएसवी) के प्रसार को सीमित करने के लिए पपीते के खेत के पास कुकुरबिट्स और सॉलनस सब्जियों जैसे वायरस मेजबान पौधों से बचते हुए और मासिक अंतराल पर नीम के तेल का छिड़काव, खरपतवार का छिड़काव और प्रणालीगत कीटनाशकों का उपयोग करते हुए रोग मुक्त रोपण के द्वारा एकीकृत दृष्टिकोण का पालन किया गया था। इस दृष्टिकोण ने पीआरएसवी की घटना को 50%-60% तक कम करने में मदद की।
प्रौद्योगिकी का प्रभाव
यह पहल खेती और प्रबंधन प्रथाओं के तहत अपनाए गए क्षेत्र के आधार पर किसानों की आय को 1,200 रुपए से 1,75,000 रुपए तक बढ़ाने में वास्तविक मददगार साबित हुई। इस पहल ने पास के गाँवों में अन्य किसानों को पपीते की खेती की ओर प्रेरित करने में उत्प्रेरक का काम किया।
रोपण सामग्री की मांग को ध्यान में रखते हुए और जनजातीय किसानों के बीच उद्यमिता विकास के अवसर को देखते हुए, भागीदारी मोड के माध्यम से क्षेत्र में उगने वाले पपीते की नर्सरी को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए, गुमला और लोहरदगा जिलों के लगभग 16 प्रगतिशील किसानों को “बेहतर पपीता नर्सरी स्थापना” पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षुओं को फलों पर भाकृअनुप-अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की जनजातीय उप योजना के तहत पॉली बैग और पपीते के बीज जैसे आवश्यक जानकारियाँ प्रदान की गईं।
अप्रैल-मई, 2020 के दौरान लोहरदगा और गुमला जिलों के लगभग 1,000 किसानों को प्रशिक्षित पपीता नर्सरी उत्पादकों द्वारा 28,000 से अधिक पपीते के बीज का उत्पादन और बिक्री की गई। पौधों को औसतन 10 रूपए प्रति पौधे की दर से बेचकर उद्यमी 3 महीने की अवधि में 12,000 रूपए का औसत लाभ कमा सकते हैं। कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान विशेष रूप से नर्सरी से अतिरिक्त आय किसानों के लिए एक वरदान रही है। इसके अलावा कार्यक्रम के तहत पपीता उत्पादकों द्वारा अर्जित लाभ ने क्षेत्र के अन्य जनजातीय किसानों के लिए भी आँख खोलने का काम किया है। झारखंड सरकार ने भी 2 साल के दौरान विभिन्न राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत जनजातीय किसानों के बीच पपीते की खेती को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। यह उम्मीद की जाती है कि वैज्ञानिक संस्थानों के द्वारा सहायता प्रदत्त वैज्ञानिक पपीता की खेती आगामी वर्षों में जिलों के प्रवासी मजदूरों के लिए एक प्रभावी आय सृजन गतिविधि साबित हो सकती है।
(स्रोत: भाकृअनुप- पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना और फलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना)
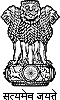







Like on Facebook
Subscribe on Youtube
Follow on X X
Like on instagram