कई तरह की बीमारियों का प्रकोप, खेती की उच्च लागत, आहार आदानों की भारी आवश्यकता और वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण कीमतों में गिरावट तटीय क्षेत्र के किसानों द्वारा झींगा पालन में सामना की जा रही चुनौतियों में से कुछ हैं।
बिचोलिम के प्रगतिशील किसान श्रीमती अनीता मैथ्यू वल्लिकापेन और उनके पति, श्री मैथ्यू वल्लिकापेन ने भाकृअनुप-केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पुराने गोवा के वैज्ञानिकों द्वारा प्रदत्त तकनीकी जानकारियों के साथ उच्च उत्पादन, आय, संसाधन साइकिलिंग एवं रोजगार के लिए सलेम, गोवा के 1.8 हेक्टेयर क्षेत्र में एक सतत एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) मॉडल (ब्लू हार्वेस्ट फार्म) विकसित किया था। मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, फलों की फसलें, सब्जियाँ, वर्मी-खाद और बायोगैस प्रणाली के घटकों में से थे।

कोविड-19 के प्रसार के दौरान, संस्थान ने एकीकृत कृषि प्रणाली को विकसित करने में किसान का मार्गदर्शन किया, जो अधिक लाभदायक, सतत और संसाधन कुशल है। वैज्ञानिकों ने अत्यधिक मूल्यवान तटीय मछली प्रजातियों - चार मीठे पानी के तालाबों (प्रत्येक 1,500 m2 में से प्रत्येक) में एशियाई सीबास (लेट्स कैल्केरिफ़र) (4,500) के साथ मोज़ाम्बिक तिलापिया (ओरियोक्रोमिस मोसाम्बिकस) (15,000) और धारीदार कैटफ़िश (भासा) (पैंगसियोडोन हाइपोफ़थलमस) (4,000) - की पॉली-कल्चर (बहुशस्यल/बहु-संस्कृति) पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया।
इस प्रक्रिया से सीबास ने 1.5 से 2.5 किलोग्राम, भासा ने 1 से 1.2 किलोग्राम और 10 महीने के बाद तिलपिया ने 300 से 400 ग्राम का औसत वजन प्राप्त किया। सीबास, तिलपिया और भासा से कुल मछली उत्पादन क्रमशः 6,000 किलोग्राम, 8,000 किलोग्राम और 6,000 किलोग्राम था। पिगरी (हैम्पशायर, लार्ज ब्लैक, क्रॉसब्रेड, अगोंडा गोअन, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, लैंडरेस और ड्यूरोक) ने 2,500 किलोग्राम प्रति माह के उत्पादन के साथ इस प्रणाली में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।



कुक्कुट पालन में, लगभग 150 पक्षियों (श्रीनिधि, वनराज और ग्रामप्रिया) को एक साथ पाला गया, प्रति मुर्गी लगभग 2 किलो वजन और प्रति पक्षी 120 अंडे का उत्पादन किया गया।
लगभग, 150 क्विंटल अनानास को केला, पपीता और शौकिया फलों के साथ नियमित रूप से उपलब्ध क्षेत्र (0.36 हेक्टेयर) से काटा गया था। सब्जियों की घरेलू जरूरतें (तेंदली, परवल, खीरा, कद्दू, लाल ऐमारैंथस, टैपिओका और एलीफेंट फुट यम) किचन गार्डन से पूरी की जाती थीं।
भोजन, फल, सब्जी एवं मुर्गे के कचरे को सूअरों और भासा को खिलाया गया और अवशेषों को खाद के लिए निर्देशित किया गया। बायोगैस इकाई में लगाया गया अपशिष्ट और सुअर के गारा/घोल का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में लिया गया। खेत से खाद का कुल उत्पादन 40 टन था, जिसमें से आधे उत्पाद का विपणन किया जाता था और शेष की आपूर्ति उर्वरक के रूप में की जाती थी।


आईएफएस ने संसाधन एवं जैविक अपशिष्ट पुनर्चक्रण को बढ़ाया, कचरे से धन का सृजन किया तथा ऑन-फ़ार्म और ऑफ़-फ़ार्म कार्बन पदचिह्नों को भी कम किया। अनुमानित वार्षिक लागत (निर्धारित एवं परिचालन) 75.4 लाख रुपए के सकल रिटर्न के साथ 29.0 लाख रुपए थी, अर्थात शुद्ध लाभ 46.4 लाख रुपए का था। खेत के लिए लाभ लागत अनुपात 2.6 होने का अनुमान लगाया गया था।
आईएफएस मॉडल को अपनाने से विविध घटकों (13 प्रकार) के कारण फसल के नुकसान का जोखिम कम हो गया और एकल फसल पद्धति की तुलना में कृषि आय दोगुनी हो गई। खेती और प्रबंधन पद्धतियों/प्रथाओं के तहत क्षेत्र के आधार पर किसानों की आय को दोगुना करने में यह पहल एक वास्तविक मददगार साबित हुई है। सफलता की कहानी किसानों को प्रोत्साहित करते हुए एक उत्प्रेरक के तौर पर कार्य करती है जो अन्य किसानों को आजीविका सुरक्षा एवं आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए आईएफएस मॉडेल अपनाने हेतु प्रेरित कर सकती है।
(भाकृअनुप-केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान, गोवा)
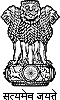







Like on Facebook
Subscribe on Youtube
Follow on X X
Like on instagram